भारत समेत कई देशों में ट्रेड यूनियनों की प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में वर्तमान में 16,000 से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियनें हैं, जिनमें से केवल 12 राष्ट्रीय स्तर की यूनियनें हैं। यह संख्या पिछले एक दशक में 20 फीसदी कम हुई है, जबकि देश का कार्यबल 50 करोड़ से अधिक हो चुका है।
श्रम ब्यूरो के 2024 के सर्वे के अनुसार, केवल सात फीसदी भारतीय श्रमिक यानी लगभग 3.5 करोड़ लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ट्रेड यूनियनों की सदस्यता पिछले 10 वर्षों में 35 फीसदी घटी है और 83 फीसदी कार्यबल असंगठित क्षेत्र में है जहां यूनियनों की पहुंच नगण्य है।
अंग्रेजी में पढ़ें : Are trade unions under threat in today's liberalised world order?
हालांकि, आजादी के बाद के दशकों में यूनियनों ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। आठ घंटे का कार्यदिवस, न्यूनतम मजदूरी कानून व कार्यस्थल सुरक्षा मानक स्थापित किए गए, लेकिन 1991 के उदारीकरण के बाद से स्थिति बदलने लगी।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े बताते हैं कि 2000-2025 के बीच हड़तालों की संख्या में 60 फीसदी की कमी आई है। 75 फीसदी से अधिक निजी कंपनियों में यूनियन गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।
गिग इकॉनमी के उभार ने स्थिति और जटिल बना दिया है। ज़ोमैटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स हैं तथा ओला या उबर ड्राइवर की संख्या 25 लाख से अधिक है लेकिन, इनमें से 95 फीसदी कर्मचारी किसी यूनियन से जुड़े हुए नहीं हैं।
एक पूर्व यूनियन नेता कहते हैं, "आज की अर्थव्यवस्था में, यूनियनें सिर्फ पांच फीसदी कर्मचारियों की आवाज बनकर रह गई हैं। हमें गिग वर्कर, फ्रीलांसर और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुंचना होगा।"
ट्रेड यूनियनों के सामने स्पष्ट विकल्प है - या तो नए आर्थिक युग के अनुकूल खुद को बदलें, या फिर धीरे-धीरे अप्रासंगिक होते चले जाएं। श्रमिक अधिकारों की यह लड़ाई अब सिर्फ कारखानों तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और घर से काम करने वाले कामगारों तक पहुंचानी होगी।
एक वैश्विक, खुली हुई अर्थव्यवस्था के दौर में ट्रेड यूनियनों की अहमियत का सवाल बड़ा होता जा रहा है। कभी क्रांतिकारी बदलाव की पेशवाई करने वाली ट्रेड यूनियनें, भारत और दूसरी जगहों पर, अपनी धार खोती हुई दिख रही हैं। वे एक ऐसी आज़ाद बाज़ार व्यवस्था में अपनी पहचान के संकट से जूझ रही हैं जहां उनकी पारंपरिक भूमिकाओं पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। निजीकरण, आउटसोर्सिंग और बढ़ती हुई गैर-संगठित कार्यबल वाली सोसाइटी में, क्या ट्रेड यूनियनें अब भी परिवर्तनकारी बदलाव के लिए इकट्ठा होने की जगह हैं, या उन्हें सिर्फ कानूनी कार्रवाई करने वाली कमेटियों तक सीमित कर दिया गया है?
भारत में, जहां ज़्यादातर कार्यबल गैर-संगठित क्षेत्र में काम करता है, पारंपरिक ट्रेड यूनियनों की अहमियत पर सवाल उठ रहे हैं। श्रम अदालतों में याचिकाओं की लंबी कतारें सीधी कार्रवाई से लंबी कानूनी लड़ाइयों की ओर बदलाव का संकेत देती हैं। हकीकत यह है कि इस खुली अर्थव्यवस्था के दौर में, मज़दूर उन नियोक्ताओं की मर्ज़ी पर हैं जो कभी भी निकाल सकते हैं। नौकरी की सुरक्षा पुरानी बात हो गई है। सरकारी विभागों द्वारा सेवाओं को आउटसोर्स करने और गिग इकोनॉमी के तेज़ी से बढ़ने के साथ, यूनियनों की सौदेबाजी की ताकत काफी कम हो गई है।
एक पूर्व ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, इस संदर्भ में सवाल उठाते हैं। “कौन किससे लड़ रहा है? ‘क्रांति के स्कूल’ के रूप में ट्रेड यूनियनें एक पुरानी अवधारणा हैं। वामपंथी एक ऐसी व्यवस्था में खुद को किनारे महसूस करते हैं जहां आर्थिक वर्ग अब मार्क्स की कल्पना के अनुसार स्पष्ट रूप से अलग नहीं हैं।“
स्व-नियोजित श्रमिकों के उदय ने शोषण की रेखाओं को और धुंधला कर दिया है, कई विक्रेता पारंपरिक नियोक्ताओं के बजाय सरकारी एजेंसियों और पुलिस को अपने मुख्य ज़ालिम के रूप में बताते हैं। एक फैक्ट्री कामगार के अनुसार, “हमारी लड़ाई सिर्फ निजी नियोक्ताओं के खिलाफ नहीं, बल्कि अधिकारियों द्वारा की जाने वाली तकलीफ के खिलाफ भी है।”
क्रांतिकारी जोश जिसने कभी ट्रेड यूनियनों को परिभाषित किया था, अब व्यावहारिकता में बदल गया है। समाजवादी टिप्पणीकार पारस नाथ चौधरी कहते हैं, “यूनियनें अपना क्रांतिकारी चरित्र खो रही हैं। प्रबंधन के साथ सौदेबाजी करने वाली कानूनी कार्रवाई समितियों में बदल रही हैं।” हड़तालें, जो कभी श्रम सक्रियता की पहचान थीं, अब दुर्लभ हैं। यूनियन नेता अक्सर प्रबंधन बोर्डों में बैठते हैं, जिन्हें औद्योगिक चक्र की रफ्तार सुनिश्चित करने का काम सौंपा जाता है, न कि उसे बाधित करने का।
कार्ल मार्क्स ने ट्रेड यूनियनों को एक समाजवादी क्रांति के लिए आयोजन केंद्रों के रूप में कल्पना की थी, जो श्रमिकों को एकजुट करते थे और उनकी वर्ग चेतना को तेज़ करते थे। हालांकि, आज, यूनियनें पूंजीवादी ढांचे को चुनौती देने के बजाय छोटे-छोटे रियायतों को हासिल करने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती हुई दिखती हैं। यह बदलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है। ट्रेड यूनियनों का क्लासिकल मॉडल—स्पष्ट वर्ग विभाजनों और सामूहिक सौदेबाजी की धारणा पर निर्मित—एक खंडित कार्यबल और सिकुड़ते नौकरी बाज़ार के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहा है।
कार्यकर्ता अजय कुमार आर्थिक अनिश्चितताओं की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, “जब विकल्प कम हों तो श्रमिक वर्ग लड़ने की हैसियत नहीं रखता,” जो सामूहिक कार्रवाई को हतोत्साहित करते हैं। राजनीतिक संस्थाओं के रूप में, ट्रेड यूनियनों का प्रभाव कम हो गया है, नेताओं ने टकराव के बजाय प्रतिष्ठान के साथ समन्वय करना पसंद किया है।
1990 के दशक तक लंबी हड़तालें आम बात थी। 1974 की जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 18 दिनों तक चलनेवाली चक्का जाम रेलवे स्ट्राइक से इंदिरा गांधी दबाव में आई और जून 1975 में इमरजेंसी लगी। लेकिन, अब पूंजीवाद खूंखार रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। पत्रकार संगठन भी खामोश हैं। अमेरिकी हायर एंड फायर सिस्टम चल चुका है। पक्की नौकरियां घट रही हैं। शोषण, अन्याय और गैर बराबरी के इस दौर में श्रमिक संगठनों को नई दिशा परिभाषित करनी होगी।















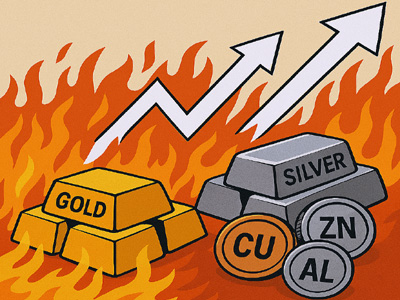
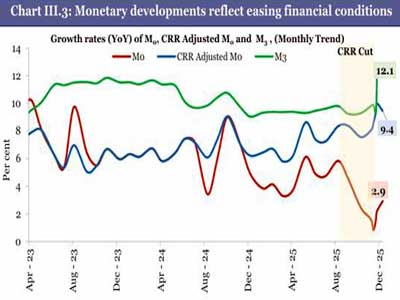

Related Items
बापू की विचारधारा और प्रासंगिकता, घटी या बढ़ी...!
राष्ट्रीय हितों के लिए गंभीर ख़तरा है विभाजनकारी राजनीति
आओ ट्रेड-ट्रेड खेलें, और बस मौज ही मौज करें...!