जब भारत चारों ओर से असहज और शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से घिरा है, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या छोटे, संसाधनहीन राष्ट्रों का कोई भविष्य बचा है? या वे हमेशा के लिए वैश्विक ‘बास्केट केस’ बनकर रह जाएंगे। खासकर, वे देश जो गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी सहायता पर निर्भरता के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, और कट्टरवाद के टापू बने हुए हैं।
तेजी से बदलती तकनीक और वैश्वीकृत बाजारों के इस युग में, सीमित श्रमबल, पूंजी की कमी और बेहद छोटे घरेलू बाजार वाले ये देश वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे हैं। वे या तो प्रवासी धन पर निर्भर हैं, या फिर क्षेत्रीय झगड़ों में उलझे रहते हैं। छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी संप्रभुता को पीछे छोड़, समेकन की ओर कदम बढ़ाना ही दीर्घकालीन हल है।
Read in English: Why nation size still matter for survival…!
यदि ये छोटे देश बड़े आर्थिक ब्लॉकों में विलीन हो जाएं, संसाधनों को साझा करें, व्यापारिक बाधाएं हटाएं, और साझा अवसंरचना विकसित करें तो वे निवेश आकर्षित कर सकते हैं, नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, और वैश्विक मंच पर अपनी सामूहिक आवाज बुलंद कर सकते हैं।
इतिहास गवाह है कि अलगाव ने हमेशा विनाश को आमंत्रित किया है, जबकि एकजुटता ने समृद्धि का मार्ग खोला है। आज का समय मांग करता है कि छोटे राष्ट्र पुरानी राष्ट्रवादी सोच से बाहर निकलें और रणनीतिक एकता के जरिए अपनी जगह बनाएं, वरना, वे धीरे-धीरे अप्रासंगिक होते जाएंगे।
तकनीक के समान अवसर देने के वादे के बावजूद, छोटे और कमजोर देशों के लिए हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। पर्याप्त भूमि, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन और पूंजी के अभाव में आत्मनिर्भर विकास की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और सब-सहारा अफ्रीका के अनेक राष्ट्र इस संकट के जीवंत उदाहरण हैं।
पाकिस्तान, जिसकी आबादी 250 मिलियन के करीब है, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन उसके पास न तो पूंजी है और न ही औद्योगिक आधार जिससे वह मुद्रास्फीति या जलवायु संकट से लड़ सके।
बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था परिधान निर्यात पर टिकी है, जो अब ऑटोमेशन और वैश्विक बदलावों के कारण खतरे में है। श्रीलंका पहले ही ऋण चूक और राजनीतिक अस्थिरता से टूट चुका है, और उसके मुख्य क्षेत्र—पर्यटन व कृषि—वैश्विक झटकों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। मालदीव, जिसकी भूमि सीमित है और जो भारी आयात पर निर्भर करता है, समुद्र के बढ़ते स्तर और वैश्विक अलगाव के दोहरे खतरे से जूझ रहा है।
छोटे राष्ट्रों के पास न तो तेल, न खनिज, न वन, और न ही जल जैसी प्राकृतिक पूंजी है, जो उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था या कूटनीति में लाभ दे सके। चाड और माली जैसे देश आज भी वर्षा-आधारित कृषि पर निर्भर हैं, जो जलवायु परिवर्तन के चलते अस्थिर होती जा रही है। मलावी और लेसोथो जैसे देशों में उपजाऊ भूमि की भारी कमी है, जिससे कुपोषण और बड़े पैमाने पर पलायन जैसी समस्याएं जन्म ले रही हैं। इन देशों में पूंजी निवेश और कुशल मानव संसाधन के अभाव के कारण, शिक्षित और कुशल लोग बेहतर अवसरों की तलाश में पलायन कर रहे हैं।
अफ्रीकी यूनियन के अनुसार, हर साल 70,000 से अधिक प्रशिक्षित पेशेवर अफ्रीका से बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान में स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना पर सरकारी निवेश बेहद कम है। बांग्लादेश की मज़दूर शक्ति विशाल होने के बावजूद, आवश्यक कौशल की कमी के कारण यह वैश्विक मूल्य श्रृंखला में पिछड़ा हुआ है।
छोटे देशों के लिए जलवायु संकट कोई भविष्य की आशंका नहीं बल्कि वर्तमान का विनाशकारी यथार्थ है। मालदीव आने वाले दशकों में डूब सकता है। बांग्लादेश हर साल बाढ़ और चक्रवात की मार से लाखों विस्थापितों को झेलता है। साहेल क्षेत्र में पानी की कमी और रेगिस्तानीकरण से हिंसक संघर्ष शुरू हो चुके हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जितनी पूंजी की जरूरत है, वह इन देशों के पास नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त वादे अधूरे रह गए हैं, और ये राष्ट्र अपनी लड़ाई अकेले लड़ने को मजबूर हैं।
भारत, चीन, और अमेरिका जैसे विशाल बाजार वाले देशों के पास झटकों को सहने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और वैश्विक नियमों को आकार देने की क्षमता है। छोटे देशों के पास यह सामर्थ्य नहीं है। वे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ‘मूल्य-निर्धारक’ नहीं, बल्कि ‘मूल्य-स्वीकारक’ बनकर रह जाते हैं।
ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल बदलावों के चलते बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों के श्रम-आधारित निर्यात क्षेत्रों पर संकट गहरा गया है। अतंर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संस्थान कुछ राहत देने की कोशिश करते हैं, पर ये उपाय स्थायी समाधान नहीं हैं। श्रीलंका में 2022 की जनता आंदोलन और पाकिस्तान का कर्ज़ संकट इस बात के प्रमाण हैं कि बाहरी ऋण और सख्त शर्तें सामाजिक अस्थिरता बढ़ा देती हैं। असल बात यह है कि जब देश छोटा हो, संसाधन सीमित हों और अर्थव्यवस्था जटिल न हो तो कर्ज़ की मदद भी सीमित हो जाती है।
भले ही ‘आकार ही सब कुछ’ न हो, लेकिन बिना आकार के सब कुछ कठिन हो जाता है। आज के प्रतिस्पर्धी और असमान विश्व में, बड़े देशों को रणनीतिक गहराई, आर्थिक विविधता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव प्राप्त है।
अब छोटे देशों के पास अब एक ही विकल्प बचता है। क्षेत्रीय एकता, मानव संसाधन में भारी निवेश, जलवायु वित्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, और पुरानी राष्ट्रवादी सोच से ऊपर उठकर साझेदारी की ओर बढ़ना। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो वे केवल संघर्ष की कहानियां बनकर रह जाएंगे।



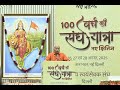













Related Items
चौंकानेवाली रही है पिछले दशक में भारत की विकास यात्रा
ट्रंप का यू-टर्न और भारत-अमेरिकी रिश्तों की सामरिक वास्तविकता
वैश्विक व्यापार संघर्ष के बीच आत्मनिर्भर भारत की राह