दोपहर की तपती धूप। सड़क किनारे सरकारी पंप। फटे-कपड़ों में एक आदमी, जिसे देखने वाले ‘भिखारी टाइप’ कह सकते हैं, महीनों बाद पानी से बदन भिगो रहा है। तभी एक चमचमाती कार रुकती है। भीतर से उतरी एक संभ्रांत महिला नाक सिकोड़कर कहती है, “देखो, कितना पानी बेकार बहा रहा है!” नहाने वाला चुप नहीं रहता। गुर्राकर जवाब देता है, “मैडम, आपके बाथटब से कम ही खर्च कर रहा हूं।” बस, यही एक पल भारत की असली कहानी कह देता है, फासला संसाधनों का नहीं, सोच का है।
यही फासला आज विकास की बहस में भी झलकता है। क्या भारत से यह कहा जा रहा है कि वह साफ़ हवा और करोड़ों लोगों को भूख से आज़ादी, इन दोनों में से किसी एक को चुने? यही डर की कहानी है, जो ज़ोर-शोर से फैलाई जा रही है। हर फ्लाइओवर तबाही की निशानी बना दिया जाता है, हर फैक्ट्री की चिमनी को क़यामत का ऐलान। मानो, तरक़्क़ी कोई गुनाह हो।
ज़रा ठहरकर देखिए। भारत की शहरी गाड़ी तेज़ रफ़्तार से आगे बढ़ रही है, थोड़ी शोरगुल वाली, थोड़ी बेतरतीब, मगर रुकने वाली नहीं। जहां कभी खेत थे, वहां अब इमारतें हैं। सड़कें दूर-दराज़ इलाक़ों को बाज़ार और मौक़ों से जोड़ रही हैं। शहर फैल रहे हैं, भीड़भाड़ वाले, अव्यवस्थित, मगर ज़िंदा।
हां, शहरों की हवा भारी है। नदियां बीमार हैं। कूड़ा बढ़ रहा है। लेकिन, इसे तरक़्क़ी बनाम तबाही की बहस बना देना बौद्धिक बेईमानी है। यह क़यामत नहीं, बल्कि बदलाव का दौर है। आर्थिक विकास ने आख़िरकार वही करना शुरू किया है, जिसका उससे वादा था, ग़रीबी को पीछे धकेलना। कारख़ाने चल रहे हैं, बंदरगाहों पर रौनक़ है, रोज़गार पैदा हो रहा है। करोड़ों लोग, जो दशकों तक हाशिए पर थे, अब मुख्यधारा का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उन्हें घर चाहिए, सड़कें चाहिए, स्कूल और अस्पताल चाहिए, सफ़र की सहूलियत चाहिए, और सबसे ज़रूरी, इज़्ज़त। क्या उनसे कहा जाए कि “पहले हवा पूरी तरह साफ़ हो जाए, तब तक इंतज़ार करो”?
शहरीकरण कोई साज़िश नहीं, एक नतीजा है। गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि शहर बुला रहे हैं। ट्रेनें तेज़ हैं, हवाई जहाज़ सस्ते हैं, मोबाइल हाथ में है। आज एक घरेलू कामगार का बेटा दिवाली पर हवाई जहाज़ से घर आता है। किसान की बेटी दूसरे राज्य में पढ़ती है। यही समावेशन है, थोड़ा अव्यवस्थित, थोड़ा शोरगुल वाला, मगर ज़रूरी। और यही बात कुछ ख़ास तबक़ों को बेचैन करती है।
‘पर्यावरण संकट’ का सबसे ऊंचा शोर अक्सर उन्हीं लोगों से आता है, जिनकी तरक़्क़ी उस दौर में हुई जब मुक़ाबला कम था। असली परेशानी हवा या पेड़ों से नहीं, हिस्सेदारी से है। जब आम लोग बराबरी मांगते हैं, तो ख़ास सुविधाएं सिकुड़ने लगती हैं। सड़कें भर जाती हैं, हवाई अड्डे भीड़ से गूंज उठते हैं, मोहल्ले बदल जाते हैं, तभी तरक़्क़ी अचानक ‘ख़तरनाक’ कहलाने लगती है।
खनन, ड्रेजिंग, इंफ़्रास्ट्रक्चर, सबको दुश्मन बना दिया जाता है। यह भुला दिया जाता है कि बिना कच्चे माल के उद्योग नहीं, बिना उद्योग के रोज़गार नहीं, और बिना रोज़गार के कल्याण भीख बन जाता है, सशक्तिकरण नहीं। विडंबना यह कि सामाजिक न्याय की बातें करने वाले लोग उसी प्रक्रिया का विरोध करते हैं, जो उसे संभव बनाती है।
हां, प्रदूषण है। झुग्गियां हैं। कचरा है। मगर भूख भी है, बेरोज़गारी भी है, और दशकों की उपेक्षा का दर्द भी। लोकतंत्र में समस्याएं पैकेज में आती हैं। हल पीछे हटना नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ना है।
डर और अतिशयोक्ति पर ज़िंदा रहने वाली विकास-विरोधी लॉबी हर चीज़ में प्रलय देखती है। एक पेड़ कटा नहीं कि सभ्यता ख़त्म। एक सड़क बनी नहीं कि ‘जन-विरोधी’ का तमगा। मोमबत्ती जुलूस तस्वीरें देते हैं, समाधान नहीं। नदियां भाषणों से साफ़ नहीं होतीं, बल्कि विज्ञान से होती हैं। धुआं नारों से कम नहीं होता, बल्कि तकनीक से होता है। और तकनीक रास्ता दिखा रही है—स्वच्छ ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहन, कचरे से ऊर्जा, स्मार्ट योजना। ये सपने नहीं, औज़ार हैं। भारत के पास लोग हैं, दिमाग़ हैं, अब संसाधन भी हैं। जिसकी ज़रूरत नहीं, वह है डर के कारण ठहर जाना।
बदलाव में तकलीफ़ होती है। हालात बेहतर होने से पहले बिगड़ते हैं। शहर चरमराते हैं। मगर अब रुक जाना निर्दयता होगी। जो लोग देर से आगे आए हैं, उनसे यह कहना कि “अभी नहीं”, यह ज़ुल्म है।
सड़क किनारे नहाता वह आदमी और बाथटब में डूबा आराम, यही भारत की असली बहस है। सवाल विकास का नहीं, सोच के फासले का है। रास्ता साफ़ है, बदलाव को अपनाइए, उसे बेहतर बनाइए, मगर उसकी राह मत रोकिए। भारत आगे बढ़ रहा है, सारी मुश्किलों के साथ। और इस बार, हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है















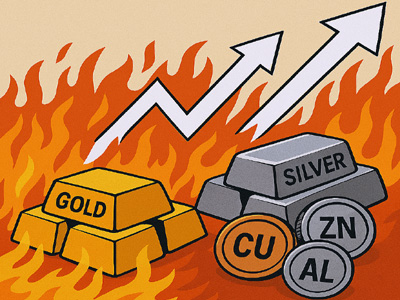
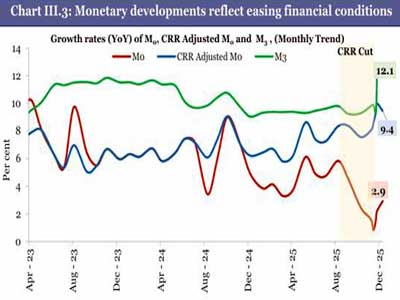

Related Items
‘विकसित भारत’ की चमक के नीचे थका हुआ आदमी…
बारिश के देवता तो हुए मेहरबान, लेकिन पानी कहां गया...?
हवाई सफर में जानलेवा लापरवाहियां और सरकारी ढकोसले!