चेन्नई शहर में, अचानक रास्ता पूछने के चक्कर में एक लैदर बेल्ट और बटुए बेचने वाले से टकराहट हुई। हमने गलतफहमी में उससे अंग्रेजी में जानकारी लेनी चाही, उसने हिंदी में बताया। बोली का लहजा कुछ जाना पहचाना सा लगने पर हमारा अगला सवाल था... कहां से हो? सकुचाते हुए वह बोला, “आगरा से हैं…”। “आगरा में कहां से?” “इटौरा के पास के गांव से…“ उसने बताया “निरे लौंडे” अपनी तरफ के यहां हैं!
दक्षिण भारत के अनेकों शहरों में, गोल गप्पे वाले, पान वाले, प्लंबर, पुताई करने वाले, यूपी, झारखंड या बिहार के हैं। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में ठेके पर काम करने वाले, कुर्ग क्षेत्र में कॉफ़ी एस्टेट पर भी तमाम बिहारी, बंगाली और उत्तर-पूर्व के लोग काम करते हैं। रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, नर्सिंग होम व होटलों में बड़ी संख्या में असम, मणिपुर व मेघालय के युवा कार्यरत हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी को थोड़ी-बहुत हिंदी आती है। चश्मे की दुकान वाले नावेद ने बताया कि ज्यादातर दक्षिणी मुसलमान हैदराबादी हिन्दुस्तानी से वाकिफ हैं, और आप केरल में भी हिंदुस्तानी में बात कर सकते हैं। वायनाड दौरे पर हमें स्थानीय लोगों से संवाद करने में कोई खास परेशानी नहीं हुई।
तो फिर समस्या क्या है? हमारे देश में भाषाएं सिर्फ़ बोलचाल का ज़रिया नहीं हैं बल्कि ये पहचान हैं, अस्मिता हैं। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा ‘दिखावटी ग़ुरूर’ की वजह भी बन जाती हैं जिससे सामाजिक विघटन और खटपट की खाई गहरी होती जाती है।
सत्तर सालों में, भाषाई दंगों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। आज़ादी के बाद से ही देश में भाषा एक ऐसा मुद्दा रहा है, जिसने कई बार राज्यों में तकरार, आंदोलन और वैचारिक जंग को जन्म दिया है।
पहली गलती जब हुई, 1956 में पंडित नेहरू ने भाषा के आधार पर संघीय इकाइयों के गठन के मनसूबे को हरी झंडी दिखाई। जब भारत ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया, तो सोचा गया था कि इससे प्रशासन आसान होगा और स्थानीय पहचान को मज़बूती मिलेगी। मगर अफ़सोस, इस फ़ैसले ने एकता की जगह अलगाव को बढ़ावा दिया। धीरे-धीरे भाषाओं का इस्तेमाल सियासी हथियार के तौर पर होने लगा।
हिन्दी को राष्ट्रभाषा के तौर पर अपनाने की कोशिशें आज तक अधूरी हैं। पचहत्तर सालों में भी दक्षिण भारत, ख़ासकर तमिलनाडु और कर्नाटक, हिन्दी को स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। वहां ‘हिन्दी थोपने’ के नाम पर कई बार ज़ोरदार आंदोलन हुए हैं। आज भी तमिलनाडु में ‘दो भाषा नीति’ को ही मान्यता है। कर्नाटक भी धीरे-धीरे उसी राह पर है।
भाषा के नाम पर राजनीति इतनी बढ़ गई है कि प्रवासियों को उनके बोली के आधार पर निशाना बनाया जाने लगा है। मुंबई में शिवसेना का उत्तर भारतीयों और हिन्दी भाषियों पर हमला कोई नया किस्सा नहीं। हाल ही में अभिनेता-राजनेता कमल हासन के तमिल, कन्नड़ भाषाओं पर एक बयान ने फिर से बहस की आग को ऑक्सीजन दी।
हक़ीक़त यह है कि भाषा को ‘तहज़ीब’ और ‘मोहब्बत’ का ज़रिया बनने के बजाय लड़ाई झगड़े, दूरियां बढ़ाने का एक खतरनाक औज़ार बना दिया गया है। नेता भाषा के नाम पर लोगों के ‘जज़्बातों’ से खेलते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और अवाम को बांटते हैं।
नई शिक्षा नीति में भी ‘तीन भाषा फ़ॉर्मूला’ को लेकर स्थिति साफ़ नहीं है। जहां एक ओर नीति में बहुभाषिकता की बात की गई है, वहीं ज़मीन पर उसके क्रियान्वयन में ढील है। दक्षिण के राज्यों को यह नीति ‘हिन्दी थोपी’ जाने की कोशिश लगती है।
मगर हक़ीक़त कुछ और कहती है। आज सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है — हिन्दुस्तानी। यह हिन्दी, उर्दू और देशज बोलियों का एक मधुर संगम है। सिनेमा, टेलीविज़न, सोशल मीडिया और आम जन-जीवन में यही ज़बान दिलों को जोड़ती है। लेकिन, अफ़सोस कि इसे भी 'उत्तर भारतीय प्रभाव' के चश्मे से देखा जाता है।
इधर, अंग्रेज़ी की बादशाहत अब भी बरक़रार है। अंग्रेज़ी सिर्फ़ भाषा नहीं, ‘रुतबा’, ‘तालीम’, और ‘तरक़्क़ी’ का रास्ता बन गई है। अंग्रेज़ी बोलने वाला आज भी समाज में क़द पाता है। निजी क्षेत्र में अच्छी नौकरी, खासतौर पर उभरते आईटी सेक्टर, हायर लेवल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी व मेडिकल आदि में अंग्रेजी ही सफलता का पासपोर्ट है। ।
समाधान शायद किसी भाषा को थोपने में नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानी जैसी स्वाभाविक, मिली-जुली ज़ुबान को अपनाने में है। एक ऐसी भाषा जो न सिर्फ़ समझ में आए, बल्कि दिल में भी उतर जाए। जो ‘ज़मीन से जुड़ी’ हो, और ‘आसमान छूने’ का हौसला भी दे...














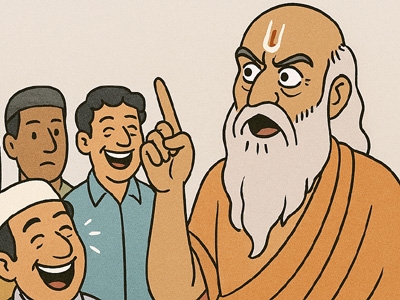
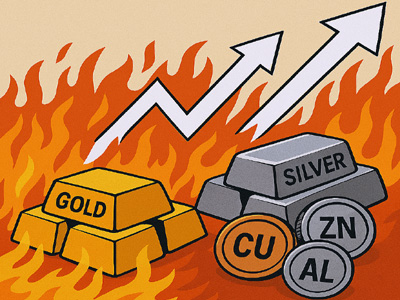
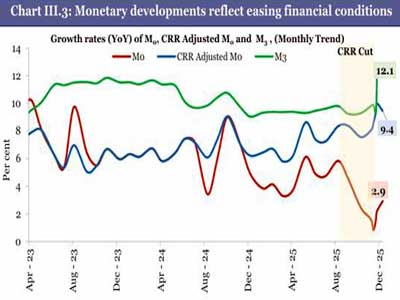

Related Items
‘जेन-जी’ की गाली-गैलेक्सी, भारत के एलीट स्कूलों में हो रहा है भाषा का पतन!
जब आगरा की सांसें धुएं और धरोहर के बीच अटक गईं…
केवाईवी गैर-अनुपालन वाले वाहनों के लिए बंद नहीं होंगी फास्टैग सेवाएं