भारत में भारी बारिश से हुई त्रासदी ने अपना कहर बरपाया है। आगरा के ऐतिहासिक ताज महल से लेकर मथुरा-वृंदावन की पवित्र भूमि तक, यमुना नदी अपने किनारों से उफनकर बाहर निकली है, जिससे भारी तबाही हुई है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानवजनित विनाश है।
लापरवाही से किए गए निर्माण, अतिक्रमण करती बिल्डर लॉबी, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ ने नदी के प्रवाह को रोक दिया। अब, उसने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिससे पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। यह प्रकृति का जवाबी हमला है, एक डरावनी चेतावनी है कि अब बहुत हो चुका।
इस वर्ष यमुना नदी में आई बाढ़ ने 1978 की तबाही और मंजर को फिर से ताजा कर दिया। गनीमत रही कि दिल्ली के ओखला बैराज की ढंग से डिसिल्टिंग हो चुकी थी जिससे जल संचय की क्षमता काफी बढ़ गई। 1997 में निर्मित गोकुल बैराज ने अपार जल प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद की। हथिनी कुंड बैराज से भी कैनाल सिस्टम में काफी पानी को डायवर्ट किया गया। इस वजह से आगरा की स्थिति इस बार उतनी गंभीर नहीं हुई, जितनी आशंका थी।
फिर भी, साल 2025 का मानसून एक बार फिर उत्तरी भारत को पानी की तबाही में डुबो गया। बेरहम बारिशों ने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आस-पास के इलाक़ों में क़हर ढा दिया। यमुना, सतलुज और ब्यास जैसी नदियां उफ़ान पर आ गईं, घरों, सड़कों और खेतों को डुबो दिया। अब तक 90 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। सिर्फ़ पंजाब में ही 43 से ज़्यादा लोग मारे गए, जो दशकों की सबसे बड़ी तबाही मानी जा रही है।
दिल्ली ने बेबसी से देखा कि यमुना ने ख़तरे का निशान पार कर लिया। कई मशहूर जगहें डूब गईं और आगरा में ताज महल की दीवारों तक पानी पहुंच गया। तक़रीबन पचास साल बाद ऐसा हुआ है। यह सिर्फ़ कुदरत का खेल नहीं है, बल्कि हमारी इंसानी ग़ुरूर, बेपरवाही और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर की सख़्त याद दिलाता है। पुरानी मान्यता है कि नदियां अपना असल रास्ता कभी नहीं भूलतीं।
सबसे बड़ा सबक़ यही है कि नदियों के किनारों और वेटलैंड्स पर क़ब्ज़ा कर हमने अपनी मुसीबत ख़ुद खड़ी की। दिल्ली में यमुना के किनारे अनियंत्रित निर्माण ने उसके रास्ते को तंग कर दिया, नतीजा यह हुआ कि पानी रिहायशी इलाक़ों में घुस आया। गुरुग्राम का हाल भी यही है — जिसे कभी ‘मिलेनियम सिटी’ कहा जाता था। वहां तेज़ शहरीकरण ने नालों और झीलों के रास्ते रोक दिए। घाटा झील और नजफ़गढ़ नाले पर क़ब्ज़ों की वजह से मामूली बारिश में भी सड़कों पर दरिया बहने लगते हैं। इस बार तो हालात और बदतर हो गए हैं।
राजस्थान में भारी बारिश ने सूखी नदियों और झीलों को ज़िंदा कर दिया। सवाई माधोपुर का सूरवाल डैम टूट गया, गांव डूबे, मगर साथ ही भूजल भी रिचार्ज हुआ। अजमेर, बूंदी और उदयपुर में सूखे नदी-नाले फिर से बहने लगे। 63 फीसदी ज़्यादा बारिश के चलते पूरे राज्य में 193 मौतें दर्ज हुईं। यह कुदरत का ‘कोर्स करेक्शन’ है, जो हमें याद दिलाता है कि इंसानी दख़ल और बेहिसाबी दोहन ने नदियों को ख़ामोश कर दिया था।
आगरा की बाढ़ ने एक और कमी उजागर की — नदियों की सफ़ाई और डिसिल्टिंग का भारी अभाव। यमुना की तलहटी गाद और गंदगी से भरी हुई है, उसकी क्षमता घट गई है। इसी वजह से पानी का दबाव बढ़ा। उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट ने पहाड़ों में भूस्खलन कर दिया, सैकड़ों घर और सड़कें मलबे में दफ़न हो गईं। यूपी में गंगा के किनारे बसे निचले इलाक़े जलभराव से जूझते रहे, क्योंकि नाले और नदियों पर क़ब्ज़ा है, रखरखाव नहीं।
यह तबाही उस ग़लतफ़हमी को तोड़ती है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब बारिश कम होना है। असल ख़तरा है बारिश के पैटर्न का बिगड़ना। अब कभी बेक़ाबू बारिश, कभी बादलों का फटना, कभी तूफ़ान। उत्तरी भारत का यह सैलाब बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन की ही चेतावनी है।
अब शहरों को नया विकास मॉडल चाहिए। गुरुग्राम जैसी बेतरतीब बस्ती नहीं, बल्कि योजनाबद्ध विकास, झीलों की बहाली, डूब क्षेत्र पर निर्माणों पर रोक, और हरियाली के इलाक़े, जो पानी सोख सकें। पंजाब और हरियाणा को सतत खेती अपनानी होगी। उत्तराखंड को पूर्व चेतावनी प्रणाली में निवेश करना होगा।
सबसे अहम बात है सरकारों का लापरवाह रवैया। देर से राहत पहुंचाना, कमज़ोर मदद, और क़ानून तोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं। हमें पहले से सतर्क होना होगा। यानी सिर्फ़ राहत नहीं, बल्कि मौसम अनुकूल नीतियां, सख़्त क़ानून और लोगों की शिरकत को भी सुनिश्चित करना होगा।
नदियां अपने ग़ुस्से से हमें सिखा रही हैं कि इंसान को विनम्र होना होगा। अगर अब भी न सुना, तो अगली बाढ़ और भी बेरहम होगी।














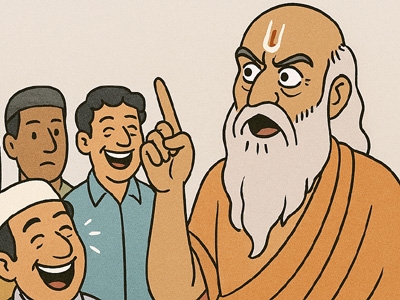
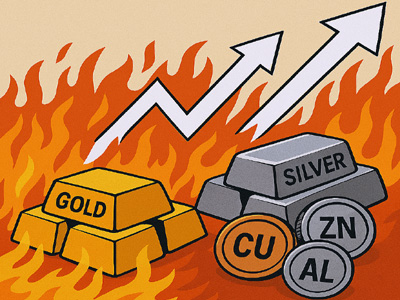
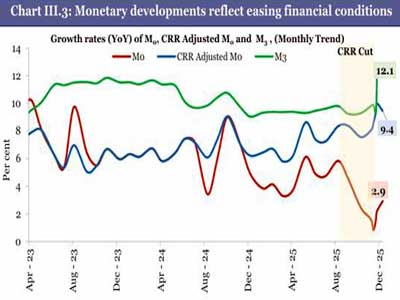

Related Items
एक गणराज्य के रूप में भारत की 'अद्वितीय' यात्रा...
कंक्रीट और कारोबारी बाजार को भेंट तो नहीं चढ़ रही पवित्र तीर्थ स्थलों की रूह!
वैश्विक चिकित्सा यात्रा गंतव्य के रूप में उभर रहा है भारत