नेपाल, बांग्लादेश और कई वर्ष पहले मिस्र में हुए छात्र आंदोलनों ने सत्ता पलट दी। हश्र यह हुआ कि वहां अभी तक लोकतंत्र मजबूती नहीं दिखा सका है। तो, क्या वजह हैं जो भारत, अमेरिका आदि देशों में लोकतंत्र इतना मजबूत है।
सबका साथ, सबका विकास, यही है राइट चॉइस ऑफ गवर्नेंस। लेकिन, कुछ अतिवादी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व पर कांग्रेसीकरण, मतलब लचरता, ढ़िलमुलपन, का इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि उनको अपेक्षा थी एक कट्टरवादी विचारधारा के फैलने फूलने की, मगर आज भारत के गुलशन में विविध रंगों के पुष्प खिल रहे हैं। यह अराजकता नहीं बल्कि ताकत है, सहनशीलता है, दूसरों को झेलने की क्षमता, तनाव और दिक्कतों में साथ जीने की ख्वाइश का इजहार है।
Read in English: Why democracy breathes only in diversity…!
विविधता ही लोकतंत्र की असली सांस है। जहां समाज बहुरंगी परतों, विचारों की टकराहट और सह-अस्तित्व से खिलता है, वहीं लोकतंत्र गहरी जड़ें पकड़ता है। विभिन्नता सिर्फ संस्कृति की खूबसूरती नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे का सुरक्षा कवच है।
इसके बरअक्स, जब समाज को एकरूपता के खोल में कैद कर दिया जाता है, जब केवल एक विचारधारा या धार्मिक स्ट्रेट जैकेट थोप दी जाती है, तो रास्ता सीधा तानाशाही और फासीवाद की अंधेरी सुरंग की ओर जाता है। इतिहास गवाह है कि विविधतापूर्ण समाज ही लोकतंत्र को जीवन देते हैं। बाकी सब अधिनायकवाद की ठंडी कब्रगाहें हैं।
कई देशों में लोकलुभावन राजनीति और तानाशाही का रंग गहरा हो रहा है। सवाल यह है कि लोकतंत्र इतनी मुश्किलों के बावजूद कहां टिकता है और कहां टूट जाता है? जहां समाज में धर्म, भाषा, जाति, इलाक़े और सोच की विविधता होती है, वहां सत्ता अपने आप जवाबदेह रहती है। हर समुदाय, हर गिरोह अपनी आवाज़ उठाता है, और सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। इसके उलट, जहाँ समाज एकरूप है, एक ही धर्म या एक जैसी सोच पर टिका है, वहां अक्सर एक ही पार्टी या एक नेता हावी हो जाता है। नतीजा—तानाशाही, एक-दलीय हुकूमत या बार-बार सत्ता पलट। या फिर हिटलर, मुसोलिनी, माओ जैसे प्रयोग।
अमेरिका 1789 से दुनिया की सबसे स्थिर लोकतंत्र की मिसाल है। यहां दुनिया के हर कोने से आए अप्रवासी बसे हैं। प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, यहूदी, मुसलमान, नास्तिक सब रहते हैं। अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन और यूरोपीय नस्लें एक साथ रहती हैं। यही विविधता समझौते को मजबूर करती है। संविधान ने शुरुआत से ही धर्म को राजनीति से अलग रखा। 1960 के दशक का नागरिक अधिकार आंदोलन याद कीजिए। अफ़्रीकी-अमेरिकी और प्रगतिशील गोरों ने मिलकर नस्लभेद की दीवारें गिराईं। अगर अमेरिकी समाज एकरूप होता, तो शायद लोकतंत्र वहां इतना जीवंत नहीं होता। आज भी वहां गर्भपात से लेकर इमिग्रेशन तक, बहसें लोकतंत्र को गतिशील बनाए रखती हैं।
भारत की मिसाल और भी दिलचस्प है। 1947 से अब तक भारत ने तमाम मुश्किलों और झटकों के बावजूद लोकतंत्र को ज़िंदा रखा। यहां 80 फीसदी से ज़्यादा आबादी हिंदू है, लेकिन संविधान ने सभी धर्मों, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्धों को बराबरी का दर्जा दिया। भारत की ताक़त उसकी इंद्रधनुषीय समाज है। यहां 22 से ज़्यादा भाषाएं हैं, अनगिनत जातियां हैं और सैकड़ों सांस्कृतिक परतें। यही विविधता किसी एक सोच या एक नेता को पूरी तरह हावी होने नहीं देती।
1975-77 की इमरजेंसी इसका सबूत है। उस वक़्त इंदिरा गांधी ने नागरिक आज़ादियां छीन ली थीं, लेकिन जनता ने 1977 में उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। लोकतंत्र फिर से बहाल हो गया।
आज भी नागरिकता क़ानून, किसान आंदोलन या चुनावी गठबंधनों के ज़रिये भारत का लोकतंत्र ज़िदगी की जिंदादिली दिखाता है। यहां वोटिंग का प्रतिशत कई विकसित देशों से ज़्यादा है।
यूरोप ने भी तानाशाही का ज़हर चखा है। जर्मनी और इटली की 20वीं सदी की तानाशाही ने उन्हें तोड़ दिया। अब वही देश सैक्युलरिज़्म और बहुदलीय व्यवस्था पर टिके हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 मुल्क अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों के बावजूद लोकतंत्र की मशाल थामे हुए हैं।
जहां समाज एक ही रंग का हो, वहां लोकतंत्र अक्सर दम तोड़ देता है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी और हान बहुसंख्या का दबदबा है। वहां उइगर मुसलमानों और हांगकांग की आवाज़ दबा दी गई है।
रूस में पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईसाई पहचान और स्लाविक एकरूपता को हथियार बना लिया है। वहां चुनाव महज़ दिखावा हैं। सऊदी अरब और ईरान में धर्म आधारित हुकूमतें हैं, जहां अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष आवाज़ें हाशिए पर डाल दी जाती हैं। पाकिस्तान में बार-बार हुए फौजी तख़्तापलटों ने लोकतंत्र को अस्थिर बनाए रखा और अब बांग्लादेश को देख लीजिए। एकरूप समाज में बातचीत और समझौते की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग एक ही पहचान से जुड़ जाते हैं, और नेता उसी का सहारा लेकर सत्ता पर क़ब्ज़ा कर लेता है।
लेकिन, विविध समाज में टकराव होते हैं, बातचीत होती है, और सैक्युलर ढांचा ज़रूरी हो जाता है। यही लोकतंत्र की असली गारंटी है। अमेरिका के संस्थापक जेम्स मैडिसन ने कहा था कि विविध समाज में अलग-अलग गुट एक-दूसरे को संतुलित करते हैं, और इस तरह किसी को तानाशाह बनने नहीं देते।
आज के दौर में लोकतंत्र की असली ताक़त विविधता में है। यही लोकतंत्र की रूह है। जहां ग़ैर-एकरूपता होगी, वहीं लोकतंत्र सांस लेगा। अगर समाज एक ही रंग में ढल गया, तो तानाशाही का ख़तरा और भी बढ़ जाएगा। इसलिए, लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है तो बहुलता और विविधता को अपनाना ही होगा। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ज़मानत और सबसे अहम पूंजी है।






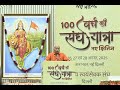










Related Items
बिहार में चुनाव, सियासी दंगल या लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा!
ट्रंप की नई साज़िश भारत के लिए शिकंजा है या सुनहरा मौक़ा!
भारत के पड़ोस में बढ़ती सियासी अस्थिरता