भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान दो अलग-अलग जंगें लड़ी गईं। एक मैदान में फौजी जवानों द्वारा, और दूसरी इंटरनेट की दुनिया में, जहां डिजिटल सूरमाओं ने सूचनाओं और झूठी खबरों की बौछार कर दी। जैसे ही ज़मीन पर गोलियां चलीं, सोशल मीडिया पर मीम्स, नकली तस्वीरें, और पक्षपाती विश्लेषणों का तूफान आ गया। एक्स, पूर्व में ट्विटर, व्हाट्सएप और अन्य मंचों पर फैलती इन बातों ने लोगों को उलझन में डाल दिया और सोच को बांट दिया।
आज का दौर जुड़ाव का है, मगर इंसानी दिमाग हर पल घिरा हुआ महसूस करता है। कनेक्टिविटी की सहूलियत ने मानवों को डिस्कनेक्टेड कर दिया है। सोशल मीडिया, न्यूज़ अलर्ट, नोटिफिकेशन, एसएमएस, कॉल्स और स्पैम ईमेल के जरिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, वह फायदेमंद कम और नुकसानदेह ज़्यादा साबित हो रही है।
इतनी अधिक जानकारी ने इंसान की समझ और सोचने की ताक़त को धुंधला कर दिया है। हर ओर से आती आधी-अधूरी और झूठी खबरों ने ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें सच्चाई और अफ़वाह में फर्क करना मुश्किल हो गया है। आज की दुनिया ने खुद एक ऐसा भस्मासुर तैयार कर लिया है, जो अब उसी को निगलने पर उतारू है।
आंकड़े भी यही बताते हैं कि एक आम इंसान रोज़ाना हजारों विज्ञापनों को देखता है, दर्जनों नोटिफिकेशन पाता है, और सैकड़ों पोस्ट के बीच अपना समय बिताता है, जिनमें से कई आपस में विरोधाभासी होती हैं। सोशल मीडिया, जिसे जोड़ने और जानकारी देने के लिए बनाया गया था, अब झूठ और सनसनी फैलाने का हथियार बन गया है।
प्रसिद्ध सामाजिक टिप्पणीकार प्रो पारस नाथ चौधरी कहते हैं, "झूठ सच्चाई से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। शोध बताते हैं कि ऑनलाइन गलत जानकारी सच्ची बातों से छह गुना तेज़ पहुंचती है। यह डिजिटल हमला लोगों को भ्रम में डाल देता है और संस्थाओं पर भरोसा कम करता है।”
झूठी खबरें दो रूपों में आती हैं। पहली ग़लत जानकारी के रूप में, जो अनजाने में फैलाई जाती हैं। और, दूसरी दुर्भावनापूर्ण जानकारियां, जो जानबूझकर भ्रमित करने के लिए फैलाई जाती हैं। इन दोनों का असर यह होता है कि आम इंसान सच्चाई को पहचान नहीं पाता है, और उलझनों में फंस जाता है। नतीजा? निर्णयहीनता। जब विकल्प बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे सामान खरीदना हो या कोई राय बनानी हो, लोग फैसला नहीं कर पाते हैं।
एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के अनुसार, बहुत सारे विकल्प होने से लोग और अधिक परेशान, तनावग्रस्त और पछतावे में जीने लगते हैं। हर समय जुड़े रहने की चाह से ‘कुछ छूट न जाए’ का डर बढ़ता जा रहा है। साल 2023 के एक अध्ययन के मुताबिक, औसत व्यक्ति दिन में 96 बार अपना मोबाइल देखता है।
नोटिफिकेशन, जिनका मक़सद जानकारी देना था, अब ध्यान भटकाने का कारण बन गए हैं। अधूरी ख़बरें और चौंकाने वाले हेडलाइन तनाव पैदा करते हैं, जबकि बिना जांचे-परखे चीज़ें शेयर करने की आदत स्थिति को और बिगाड़ देती है।
हाल की डिजिटल जंग में सैनिकों की मूवमेंट और हताहतों की अफवाहें वायरल हो गईं, जिससे पहले डर और ग़ुस्सा फैला, बाद में सच सामने आया। इसका असर सिर्फ इंसान पर नहीं, पूरे समाज पर होता है। जब जानकारी का शोर बढ़ जाता है, तो सोचने-समझने और तर्कपूर्ण चर्चा की जगह नहीं बचती। सरकारें, जो पहले सूचना की संरक्षक थीं, अब झूठ की लहर के सामने खुद को बेबस पा रही हैं।
पहलगाम की घटना के बाद सोशल मीडिया पर जो तूफान आया, उसने दिखा दिया कि कैसे एक कहानी बिना सच जाने फैल सकती है। बॉट्स और दुश्मन मानसिकता वाले लोग इसे और हवा देते हैं, जबकि प्रशासन गड़बड़ी संभालने में देर कर देता है।
तो अब किया क्या जाए? इसके लिए अब हर व्यक्ति को अपनी डिजिटल खपत पर नियंत्रण रखना होगा। नोटिफिकेशन कम करने होंगे, कुछ भी साझा करने से पहले जरूरी जांच करनी होगी। सोशल मीडिया मंचों को पारदर्शिता बढ़ानी होगी। संदिग्ध पोस्ट को चिह्नित करें, और गलत खबरों को फैलने से रोकें। सरकार को मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि नागरिक खुद सोच और समझ सकें।
यह लड़ाई खुद से बनाए एक राक्षस के खिलाफ़ है। अगर हमने अब कदम नहीं उठाए, तो शोर का कोलाहल हमारी सोच को पूरी तरह डुबो देगा। इस दुनिया में जहां जानकारी एक साथ हथियार और ढाल दोनों है, समझदारी से इसका इस्तेमाल ही हमें अराजकता से बचा सकता है।














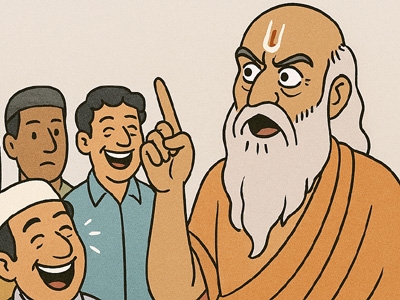
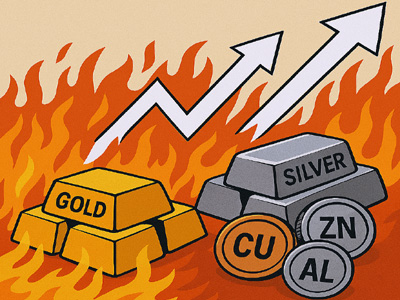
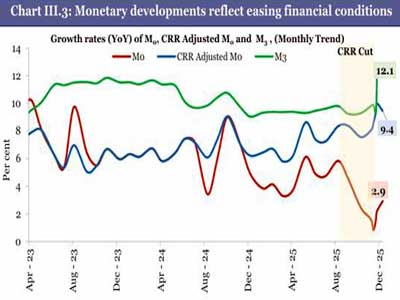

Related Items
यमुना नदी क्रूज पर्यटन स्थानीय लोगों को बनाएगा सशक्त
सोने की शक्ल में लॉकर में कैद हमारा अर्थ तंत्र...!
धर्मस्थल से उन्नाव तक झूठी ख़बरों का जुनून