रात के सन्नाटे में जब घरों की रोशनी बुझ जाती है, तब भी लाखों युवाओं की आंखें चमकती स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। अनगिनत नोटिफिकेशन्स की खनक मानसिक जंजीर बन चुकी है।
रिश्ते, जो कभी संवाद और विश्वास पर टिके थे, अब ‘सीन’ और ‘लास्ट सीन’ की दुनिया में बिखर रहे हैं। लाइक और इमोजी ने सच्चे अहसासों की जगह ले ली है, और गैजेट की गिरफ्त में कैद यह पीढ़ी गहरे ‘इमोशनल ब्लैकहोल’ में खिंचती चली जा रही है—जहां साथी तो बहुत हैं, पर वास्तविक जुड़ाव गायब है।
पुरानी पीढ़ी के लोग हर समस्या का निदान ‘लिंग पृथक्करण’ में ढूंढते हैं। उनका मानना है, “लड़के-लड़कियां हर वक्त साथ रहेंगे तो लफड़े होंगे ही।” उनके अनुसार, सह-शिक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की नीति इस इंटरनेट युग में युवा छात्रों के लिए तनाव का कारण बन रही है।
सामाजिक विचारक प्रो. पारस नाथ चौधरी मानते हैं कि कम उम्र में ही ‘बॉयफ्रेंड’ या ’गर्लफ्रेंड’ रखना फैशन बन गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म संवाद को चौबीसौ घंटे का मामला बना देते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया न मिलने से गलतफहमियां, ब्रेकअप और तनावपूर्ण रिश्ते पनपते हैं—और यह तनाव अक्सर कक्षा में ही साथ बैठे व्यक्ति से जुड़ा होता है। समस्या की जड़ पश्चिमी रिश्तों के मॉडल को परंपराओं से बंधे दकियानूसी भारतीय समाज पर थोपना है।
आजकल बड़ी संख्या में माता-पिता भी सह-शिक्षा संस्थानों से असंतुष्ट हैं, जहां छात्रों का ध्यान नैतिक मूल्यों से अधिक रूप-रंग और रिलेशनशिप पर केंद्रित हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी अय्यर का मानना है कि भारतीय समाज अभी इतनी तेज़-रफ़्तार लैंगिक समानता को आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जमाने में इतना फैशन या सजने संवरने में वक्त जाया नहीं होता था, आजकल तो छठी क्लास का बच्चा भी पेयरिंग कर रहा है, डेली डियो और परफ्यूम, छिड़क के स्कूल जाते हैं इंप्रेस करने के लिए।
आज की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा शगल बन गया है चैटिंग—व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पर घंटों फटाफट शेयरिंग। दोस्ती की शुरुआत से लेकर इज़हार-ए-मोहब्बत तक सब मोबाइल स्क्रीन पर सिमट गया है। लगातार रिप्लाई देने की मजबूरी, ‘सीन’ होकर भी जवाब न आने का डर, या प्राइवेट चैट लीक होने की आशंका—ये सब मिलकर युवाओं को भावनात्मक असुरक्षा और मानसिक दबाव की गिरफ्त में ले रहे हैं। रिश्तों में भरोसे की जगह शक और तुलना हावी हो रही है।
इसी तनाव की जड़ में है छात्रों की आत्महत्या की चौंकाने वाली दर—कुल आत्महत्या मामलों का 7.6 फीसदी यानी लगभग 13 हजार छात्र हर साल। विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, बल्कि उच्च दबाव वाला, प्रतिस्पर्धी और भावनात्मक रूप से असमर्थनशील शैक्षिक माहौल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भी इसे ‘अनदेखी गई मनोवैज्ञानिक पीड़ा, शैक्षिक अतिभार, सामाजिक कलंक और संस्थागत असंवेदनशीलता’ का नतीजा मानता है।
आज की शिक्षा प्रणाली बच्चों को रटंत और अंकों के पीछे दौड़ने पर मजबूर करती है, लेकिन उन्हें विफलता, निराशा या अनिश्चितता का सामना करना नहीं सिखाती। एक मनोचिकित्सक के शब्दों में, “हम बच्चों को परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, जीवन के लिए नहीं।”
इसलिए असली समस्या कक्षा में लड़के-लड़कियों की मौजूदगी नहीं, बल्कि एक सहयोगी और भावनात्मक रूप से सहारा देने वाले शैक्षिक ढांचे का अभाव है। मानसिक स्वास्थ्य संकट दरअसल शिक्षा व्यवस्था की गहरी कमजोरी का लक्षण है।
अंततः, ज़रूरत है एक ऐसी प्रणाली की, जो लिंग की परवाह किए बिना, सहनशील, रचनात्मक और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों का निर्माण करे—क्योंकि यही पीढ़ी कल समाज को दिशा देने वाली है।














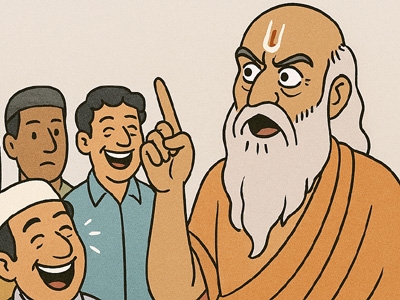
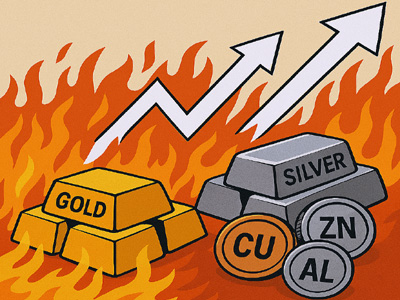
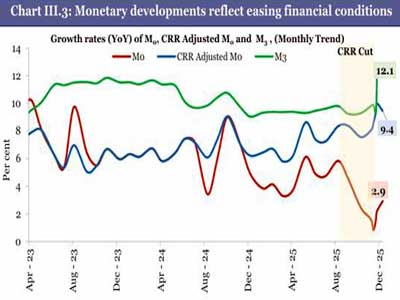

Related Items
सूखे खेतों की दरारों से झांकती रोशनी की किरण...
मानसिक स्वास्थ्य को समझने की भारतीय पहल
डिजिटल ताल पर थिरक रहा है भारत का त्योहारी व्यापार