भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल देशों में से एक है, और इसकी प्रगति में इंटरनेट कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह उपलब्धि इस साल अप्रैल से जून के दौरान दर्ज की गई 1,002.85 मिलियन इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में परिलक्षित होती है, जो भारत की डिजिटल क्रांति के पैमाने और प्रभाव को बताती है।
हालांकि, देश के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच सीमित है, जिससे मौजूदा नेटवर्क के पूरक के रूप में सैटेलाइट इंटरनेट की आवश्यकता पर बल मिलता है। सैटेलाइट इंटरनेट, भूस्थिर कक्षाओं या गैर-भूस्थिर कक्षाओं में स्थित उपग्रहों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवा है।
अंग्रेजी में पढ़ें : Satellite internet emerges as key enabler of digital connectivity
डिजिटल रूप से समावेशी राष्ट्र के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने के लिए, सैटेलाइट इंटरनेट एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें अंतरिक्ष से किसी भी स्थान तक कनेक्टिविटी प्रदान करने की क्षमता है। यह इसे दूरदराज के गांवों, पहाड़ी इलाकों, सीमावर्ती क्षेत्रों और द्वीपों के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाता है, जहां स्थलीय इंटरनेट सेवाओं तक पहुंचना या तो मुश्किल है या आर्थिक रूप से अव्यावहारिक है।
हाल ही में, सरकार ने उपग्रह संचार को नियंत्रित करने के लिए एक प्रगतिशील नियामक ढांचा पेश किया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और स्पेक्ट्रम प्रबंधन के साथ नवाचार का संतुलन बनाना है। इन नीतिगत उपायों से निजी भागीदारी, सुव्यवस्थित अनुमोदन और कुशल स्पेक्ट्रम उपयोग के लिए एक वातावरण तैयार हो रहा है, जिससे सैटेलाइट इंटरनेट को बड़े पैमाने पर अपनाने का मार्ग भी खुल रहा है।
ध्यान रहे, साल 2020 में, सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के द्वार खोलने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार लागू किए थे। इसे आगे बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 ने अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए एक समान अवसर मुहैया कराए, जिससे अंतरिक्ष गतिविधियों की संपूर्ण वैल्यू चेन में उनकी भागीदारी को शुरू से अंत तक सक्षम बनाया जा सके।
इस साल, मई के महीने में, ट्राई ने सैटेलाइट बेस्ड वाणिज्यिक संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन हेतु नियमों और शर्तों पर अपनी सिफ़ारिशें जारी कीं ताकि स्पेक्ट्रम उपयोग में लचीलेपन और दक्षता के साथ नियामक ढांचे में संतुलन स्थापित किया जा सके। ट्राई की प्रमुख सिफ़ारिशों में से एक यह है कि उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटन पांच वर्षों की अवधि के लिए किया जाए, जिसे बाज़ार की स्थितियों के आधार पर दो अतिरिक्त वर्षों तक बढ़ाने का विकल्प दिया जा सकता है।
भारत का उपग्रह संचार पारिस्थितिकी तंत्र एक परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। पारंपरिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अन्य उपग्रह ऑपरेटरों की श्रृंखला के भूस्थिर उपग्रह पर निर्भर रहने वाला यह क्षेत्र अब अधिक सक्रिय निजी भागीदारी और अगली पीढ़ी की निम्न पृथ्वी कक्षा और मध्यम पृथ्वी कक्षा उपग्रह प्रणालियों को अपनाए जाने का गवाह बन रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के क्रियान्वयन के साथ, भारत डिजिटल इंडिया के एक प्रमुख चालक के रूप में उपग्रह इंटरनेट का उपयोग करने के लिए तैयार है।
सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, आवृत्ति बैंड आवश्यक माध्यमों के रूप में कार्य करते हैं जिनके माध्यम से पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच ध्वनि, डेटा और ब्रॉडबैंड सिग्नल प्रसारित होते हैं। दूरस्थ और असेवित क्षेत्रों में कम विलंबता, उच्च बैंडविड्थ और अधिक विश्वसनीय कवरेज की आवश्यकता को देखते हुए भारत अपने सैटेलाइट इंटरनेट परिदृश्य को भूस्थिर पृथ्वी कक्षा उपग्रहों से निम्न पृथ्वी कक्षा और मध्यम पृथ्वी कक्षा प्रणालियों की ओर पुनर्परिभाषित कर रहा है। यह परिवर्तन देशभर में तेज़ और अधिक विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
निम्न पृथ्वी कक्षा सैटेलाइट आमतौर पर 400 से 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के निकट परिक्रमा करते हैं। उनकी निकटता कम विलंबता संचार की अनुमति देती है, जिससे वे इंटरनेट सेवाओं के लिए आदर्श बन जाते हैं।
मध्यम पृथ्वी कक्षा उपग्रह 8,000 से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर संचालित होते हैं। ये निम्न पृथ्वी कक्षा सैटेलाइट की तुलना में बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं और इनकी विलंबता निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रहों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के क्रियान्वयन के साथ, सरकार अब स्वचालित और सरकारी अनुमोदन मार्गों के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न खंडों में 100 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देती है, जिससे निजी भागीदारी के लिए प्रवेश मानदंड उदार हो जाते हैं, जो भारत के सैटकॉम परिदृश्य में परिवर्तन का प्रतीक है।
देश के डिजिटल कनेक्टिविटी परिदृश्य को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को जून में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने का लाइसेंस मिला है। इससे पहले, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस लिमिटेड और वनवेब इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को ऐसी सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस दिया जा चुका है।
अप्रैल तक, 10 से ज़्यादा उपग्रह ऑपरेटरों ने इसमें रुचि दिखाई है और भारत में उपग्रह क्षमता प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के लिए आवेदन किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों का प्रवेश, ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पूरे देश में उच्च गति वाले उपग्रह ब्रॉडबैंड के निर्बाध प्रसार का आधार तैयार करता है। सैटकॉम का परिवर्तनशील परिदृश्य नवाचार और अगली पीढ़ी की तकनीकों को बढ़ावा देने पर सरकार के ध्यान को रेखांकित करता है।
सरकार ने देश के सुदूर इलाकों तक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिससे व्यक्ति और समुदाय दोनों ही सशक्त हो रहे हैं। आज के डिजिटल युग में, ऐसी कनेक्टिविटी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच आसान होती है।
डिजिटल भारत निधि के तहत, सरकार 4जी सैचुरेशन परियोजना के तहत देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में 4जी मोबाइल टावरों की स्थापना के माध्यम से ब्रॉडबैंड सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, डीबीएन उन परियोजनाओं के वित्तपोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो वंचित क्षेत्रों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करती हैं।
सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए द्वीपों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना लागू की है। बीएसएनएल द्वारा कार्यान्वित उपग्रह बैंडविथ वृद्धि ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्षमता को 2 जीबीपीएस से बढ़ाकर 4 जीबीपीएस और लक्षद्वीप में 318 एमबीपीएस से बढ़ाकर 1.71 जीबीपीएस कर दिया है। यह उपग्रह वृद्धि पूरे द्वीप समूह में सुदृढ़ दूरसंचार सेवा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए फाइबर केबलों का पूरक है।
सरकार ने वंचित आबादी तक मोबाइल नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे गांवों और क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सीटीडीपी लागू किया है। जून 2025 तक, 2,485 मोबाइल टावर चालू हो चुके हैं, जो 3,389 स्थानों को मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं।
एनबीएम 1.0 के सफल समापन के बाद, 17 जनवरी को एनबीएम 2.0 की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य देशभर के शेष 1.7 लाख गांवों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाना है। एनबीएम 2.0 का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के एक नए युग में ले जाना है।
डीबीएन के तहत वित्त पोषित, भारतनेट एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को किफायती हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान करना और शहरी और ग्रामीण समुदायों के बीच की खाई को पाटना है। इस परियोजना के उपग्रह घटक का कार्यान्वयन बीबीएनएल और बीएसएनएल द्वारा दूसरे चरण के तहत किया जा रहा है। अब तक, 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें भारतनेट परियोजना से जुड़ चुकी हैं, जिनमें से बीएसएनएल 1,408 और बीबीएनएल 3,753 ग्राम पंचायतों को कवर कर रहा है।
प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पूरे भारत में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का एक नेटवर्क बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को किफायती और विश्वसनीय इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध कराना, डिजिटल भागीदारी और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना है। सितंबर तक, देश में 3.73 लाख से ज़्यादा पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जा चुके हैं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की है। यह चरम मौसम की घटनाओं के लिए समय पर और प्रभाव-आधारित पूर्व चेतावनी देने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग करती है। यह प्रणाली ऐतिहासिक आंकड़ों, वास्तविक समय के अवलोकनों, रडार और उपग्रह चित्रों पर आधारित है। यह आपदा-प्रवण राज्यों को जोखिमों की निगरानी करने और जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए उपाय करने में मदद करती है।
ये सभी प्रयास डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए उपग्रह संचार को नियोजित करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
इसरो द्वारा विकसित उच्च-थ्रूपुट उपग्रहों के माध्यम से भारत की ब्रॉडबैंड पहुंच लगातार बढ़ रही है, जो तेज़ गति और उच्च क्षमता प्रदान करने के लिए उन्नत स्पॉट-बीम तकनीक का उपयोग करते हैं। भारत के पास 19 परिचालन संचार उपग्रहों का बेड़ा है, जिनमें GSAT-19, GSAT-29, GSAT-11 और GSAT-N2 विशेष रूप से भारत की ब्रॉडबैंड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं। इन उपग्रहों को कम सेवा वाले क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने, उड़ान के दौरान संचार, रक्षा नेटवर्क और आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये उपग्रह मिलकर भारत में उपग्रह-आधारित ब्रॉडबैंड अवसंरचना की रीढ़ हैं और भारतनेट जैसे भू-आधारित नेटवर्क के पूरक हैं।
कुल मिलाकर, विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप, उपग्रह इंटरनेट डिजिटल कनेक्टिविटी के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में उभर रहा है, जो दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों तक विश्वसनीय पहुंच प्रदान करता है, साथ ही रक्षा और आपदा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को सशक्त बनाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शक्ति के माध्यम से, भारत अंतरिक्ष-आधारित संचार में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और नेतृत्व को सुदृढ़ कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कनेक्टिविटी का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। एचटीएस के संचालन से लेकर उपग्रह संचार में निजी भागीदारी को सक्षम करने तक, देश लगातार अपने डिजिटल विभाजन को लगातार पाट रहा है।














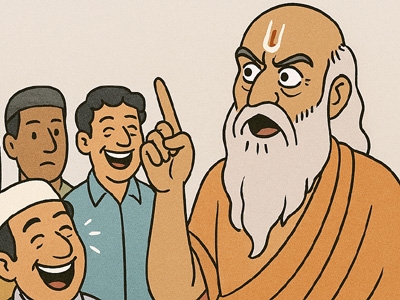
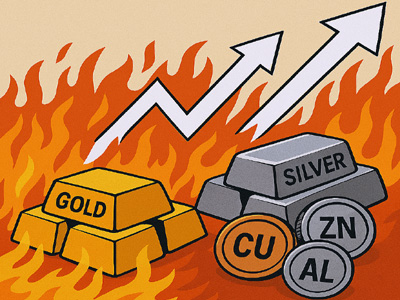
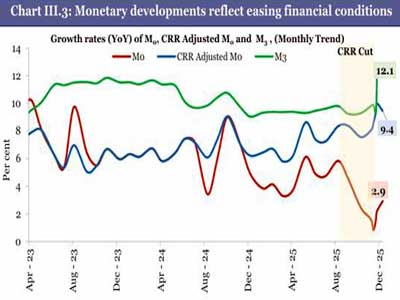

Related Items
एक गणराज्य के रूप में भारत की 'अद्वितीय' यात्रा...
वैश्विक चिकित्सा यात्रा गंतव्य के रूप में उभर रहा है भारत
‘विकसित भारत’ की चमक के नीचे थका हुआ आदमी…