यदि दैनिक जीवन में बोले जानी वाली गंदी और अपमानजनक भाषा का उपयोग करने की बात करें तो शिक्षा, संस्कृति और सम्पन्नता कोई बंधन नहीं हैं।
एक नजर से देखें तो लिंग विशेष को लक्षित करने वाली गालियां समाज के लोगों द्वारा बेशर्मी से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में एक अलग स्वाद और रंग जोड़ती हैं। इसके चलते, इस भाषाई प्रदूषण से लोग न परेशान हैं और न ही विवश। महिलाएं भी पुरुषों की ही तरह अपमानजनक भाषा का उपयोग करने में निपुण हैं। उम्र भी कोई बाधा नहीं है।
Read in English: Why do people prefer to target women with abuses?
पुराने दिनों में, लोग अपनी अभिव्यक्ति को सजाने के लिए मुहावरों, कहावतों व दोहों आदि का इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्रोध और हताशा का स्तर बढ़ने के साथ, यौनोन्मुख संवाद दिन का क्रम बन गया है।
आम लोगों के बीच गाली-गलौज और अपशब्द सामाजिक मानदंडों और कुंठाओं के आकर्षक प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जब वाक्पटुता लड़खड़ाती है, तो कई लोग अभिव्यक्ति के साधन के रूप में अभद्र भाषा का सहारा लेते हैं और हर वाक्य में ‘मां की’, ‘बहन की’ करके या शारीरिक अंगों को निशाने पर लेकर अपना आक्रोश प्रकट करते हैं।
गाली-गलौज या अपशब्दों का उपयोग अक्सर गुस्से और हताशा के लिए एक वैध निकास के रूप में किया जाता है। जैसे-जैसे लोग रोज़मर्रा की कठिनाइयों और व्यवस्थागत अन्याय से जूझते हैं, वैसे-वैसे गाली-गलौज एक भाषाई सहारा बन जाती है, जो उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देती है।
हालांकि, इन अपमानों के भीतर महिलाओं को निशाना बनाने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाना बेहद जरूरी है। इस संदर्भ में अपमानजनक भाषा का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी लैंगिक प्रकृति है। गालियों में माताओं, बहनों और बेटियों का बार-बार आह्वान महिलाओं के प्रति घृणा और महिलाओं के वस्तुकरण के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। किसी का अपमान करने के लिए पारिवारिक संदर्भों का उपयोग करके, वे न केवल अपने लक्ष्य को नीचा दिखाते हैं, बल्कि महिलाओं को एक ऐसी वस्तु के रूप में परेशान करने वाला दृष्टिकोण भी पेश करते हैं, जिसे विवादों में घसीटा जा सकता है।
सार्वजनिक टिप्पणीकार पारस नाथ चौधरी का हाल ही में दावा है कि गाली-गलौज सामाजिक परिवर्तन के लिए एक अहिंसक उपकरण के रूप में कार्य करती है। गाली-गलौज अभिव्यक्ति के एक ऐसे रूप में सामने आती है जो यथास्थिति को चुनौती देती है। उनका मानना है कि गाली-गलौज में मुहावरों और कहावतों की परिष्कृतता की कमी हो सकती है, लेकिन यह व्यवस्थागत उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रामाणिक प्रतिक्रिया का प्रतीक है।
गाली-गलौज की गहराई की खोज करने वाले एक विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किए गए शोध ने समाजभाषाई अध्ययनों में इस तरह की गाली-गलौज की भूमिका को पहचानने में एक महत्वपूर्ण क्षण को रेखांकित किया है।
यह बढ़ती अकादमिक रुचि न केवल यह समझने की दिशा में बदलाव का संकेत देती है कि क्या कहा जाता है, बल्कि यह भी कि भाषा - विशेष रूप से गाली-गलौज - आम लोगों के बीच संचार का एक स्थायी पहलू क्यों बनी हुई है।
दैनिक जीवन में गाली-गलौज इतनी आम हो चुकी है कि उनका वास्तविक अर्थ व जोर खो गया है। हर गाली में मां, बहन, बेटी को निशाना बनाया जाता है। जीजा या साला को एक विनम्र गाली माना जाता है। सामाजिक विचारक टीपी श्रीवास्तव कहते हैं कि समाज को गोलियों से नहीं बल्कि गालियों से बदलना होगा। भारत जैसे अहिंसा-प्रेमी समाज में गालियों के माध्यम से क्रोध व्यक्त करना उचित है। वास्तव में, गालियों का विस्तार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से एलजीबीटी समुदाय के अनुकूल गालियां तैयार की जानी चाहिए।
वह याद दिलाते हैं कि हिंदू समाज में गाली-गलौज बहुत पहले से मान्य हैं। शादी-ब्याह में महिलाएं गलियों से बारातियों का स्वागत करती हैं। लोग इसका आनंद लेते हैं। गली-मोहल्लों की मिली-जुली संस्कृति गालियों से सजी होती है। अगर पुलिस में नौकरी करनी है तो गाली-गलौज में पारंगत होना जरूरी है। खुशकेट अकबराबादी ने सालों पहले लिखा था, "जो गाली-गलौज नहीं जानता, उसका जीवन सूना है।"
संस्कृति विशेषज्ञ उधम पंडित इस बात से दुखी हैं कि पश्चिमी प्रभाव ने गाली-गलौज संस्कृति को काफी नुकसान पहुंचाया है। युवा वर्ग केवल "ओह शिट" आदि का ही प्रयोग कर रहा है, शायद अंग्रेजी शब्द कोष में ज्यादा ‘वैरायटी’ नहीं है।
बहरहाल, “बोलचाल की भाषा में गालियों से ‘करेंट’ और ‘बोल्डता’ आती है, इसलिए चलने दो…”, कम से कम ज्ञानी लोगों का तो यही मानना है।














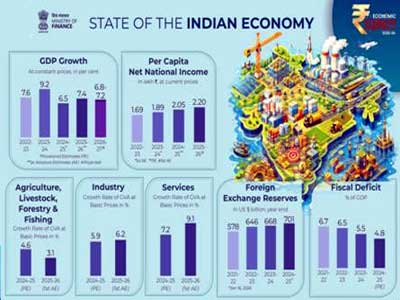



Related Items
‘जेन-जी’ की गाली-गैलेक्सी, भारत के एलीट स्कूलों में हो रहा है भाषा का पतन!
जब भाषा बन जाए तकरार और फासलों की वजह…
एकल-उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ अब बड़ी जंग की जरूरत